
Indian Political GK
Your all Nead Is done.
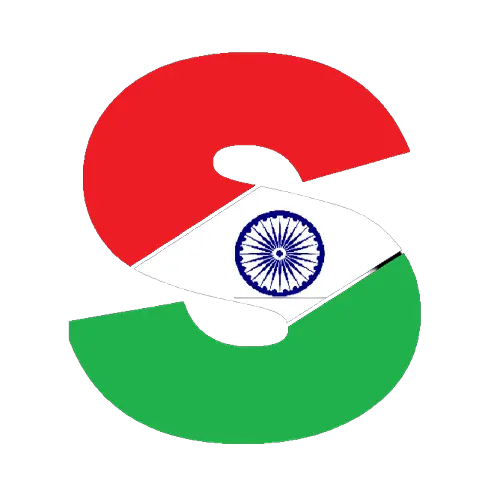
✨ सविंधान की सामान्य परिभाषा - ऐसे मौलिक नियम और सिद्धांत जो कानून के रूप में बने होते है और सबके लिए सामान होते हैं । भारतीय सविंधान के निर्माण का काम 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन तथा उसके बाद 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहा तत्पश्चात भारतीय संविधान सभा ने इसको मूर्त रूप प्रदान किया तथा देश का कानून रूप मान कर इसे लागू कर दिया ।
 ✥ 26 नवम्बर 1949 को परित तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जिसे निर्मित होने में 2वर्ष 11माह 18दिन का समय लगा था । भारत संप्रभुता संपन्नराष्ट्र है जिसका अभिप्राय है की भारत किसी विदेशी या आंतरिक शक्ति के अधीन नहीं है बाल्की सीधे देश की जनता के द्वारा चुनी गई एक मुक्त सरकार के द्वारा शासित राष्ट्र है
✥ 26 नवम्बर 1949 को परित तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जिसे निर्मित होने में 2वर्ष 11माह 18दिन का समय लगा था । भारत संप्रभुता संपन्नराष्ट्र है जिसका अभिप्राय है की भारत किसी विदेशी या आंतरिक शक्ति के अधीन नहीं है बाल्की सीधे देश की जनता के द्वारा चुनी गई एक मुक्त सरकार के द्वारा शासित राष्ट्र है
भारतीय संविधान की विशेषताएं -
1. दोहरी नागरिकता के स्थान पर भारत में एकल नागरिकता का अनुबंध ।
2. राज्यों का अपना पृथक कानून न होकर केवल एक ही संविधान का उपयोग करना ।
3. वित्तीय आपात काल के दौरान राज्यों के वित् पर केंद्र का नियंत्रण होना ।
4. भारत का संविधान विश्व का सबसे लम्बा लिखित संविधान हैं ।
✥ सर्वप्रथम 1922 में महात्मा गांधी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के बारे में बात की थी । जबकि अंग्रेजो ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव के जरिये सर्वप्रथम ये स्वीकार किया की भारतियों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जो की भारत के संविधान को निर्मित करेगी, लेकिन इस प्रस्ताव को भारतियों ने अस्वीकार कर दिया जिसका मूल कारण था कि इस प्रस्ताव में ये लिखा गया था कि इस संविधान सभा में मुख्यतया भारतीय लोग शामिल होंगे । अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का प्रमुख कारण था कि इसमें भारतीय लोगो के अलावा बहुत सारे अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं जिसमें सम्भवतया अंग्रेज भी क्यों न हो ।
☞ क्रिप्स प्रस्ताव -✥ स्टैफोर्ड क्रिप्स ने 1942 में भारतियों के सामने क्रिप्स प्रस्ताव को रखा गया जिसमे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया की भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी लेकिन इसको भी भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया था क्योंकि इसमें उल्लेखित था की युद्ध की समाप्ति के पच्छात संविधान सभा का गठन किया जायेगा । गौरतलब हैं की तत्कालीन समय में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था । इसी प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने "पोस्ट डेटेड चेक" की संज्ञा दी थी ।
☞ कैबिनेट मिशन-✥ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली की सरकार बनी । एटली ने अपने मंत्रीमंडल के 3 मंत्रियों के समुह को एक प्रस्ताव के साथ भारत भेजा जिसे हम केबिनेट मिशन के नाम से जानते है । सर पेट्रिक लोरेन्स कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष तथा स्टैफोर्ड क्रिप्स व ए.वी. एलेक्जेंडर इसमें सदस्य थे तथा इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था । ☞ संविधान सभा comming soon...
✥ भारतीय संविधान में आंतरिक और बाहरी स्रोत का उपयोग करके संविधान निर्माताओ ने इसे विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान का रूप प्रदान किया है । आंतरिक स्रोत के अन्तर्गत वो कानून या अधिनियम आते है जो अंग्रेजों ने भारत में शासन को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए किर्यान्वित किये थे, तथा उन्ही नियमों/कानूनों में से कुछ कानूनों को बाद में भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया । इसके अतिरिक्त भारत के संविधान में कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें भारतीय संविधान सभा ने विदेशी सविंधानो का अध्ययन करके उनको भारत के संविधान में शामिल कर लिया था ।
1. आंतरिक स्रोत -✥ तात्कालिक समय में संविधान सभा को सीमित समय में सर्वश्रेष्ठ संविधान को निर्मित करके गुलामी की जंजीरों से मुक्त होना था जिस कारण संविधान निर्माताओं ने 70-75% अधिनियम/कानून भारत शासन अधिनियमों से यथासम्भव संशोधित करके भारतीय संविधान में शामिल कर लिए जिनमे 1935 के भारत शासन अधिनियम के कानून सर्वाधिक मात्रा में शामिल किये गये । 326अनुच्छेद वाले 1935 के भारत शासन अधिनियम में से तक़रीबन 250अनुच्छेद यथासंभव संशोधित करके भारतीय संविधान में शामिल कर लिए गए । भारत शासन अधिनियम के तहत लोकसेवा आयोग, किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यालय, न्याय पालिका, संघीय शासन प्रणाली, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों में बंटवारे जैसे अहम कानून थे जो भारतीय संविधान में शामिल किये गये ।
2. बाह्य स्रोत -✥ भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में कुछ कानून अन्य संप्रभु राष्ट्रों के संविधानो का अध्ययन करके जोड़ा हैं जो की निम्नलिखित हैं -
i. ब्रिटेन के संविधान सेa. एकल नागरिकता का उपबंध
b. संसदीय व्यवस्था
c. विधि/कानून के निर्माण की प्रक्रिया
d. द्विसदनात्मक व्यवस्था
ii. फ्रांस के संविधान सेa. गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था
b. स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व शब्द
iii. अमेरिका के संविधान सेa. मूल अधिकार
b. स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली
c. न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था
d. राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया
e. उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था
f. प्रस्तावना की लाइन - हम भारत के लोग, की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से ली गयी हैं ।
g. वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था
iv. आयरलैंड के संविधान सेa. नीति निर्देशक तत्व
b. राष्ट्रपति के निर्वासन की पदति
c. राजयसभा में कला, साहित्य, समाज सेवा तथा विज्ञान के क्षेत्र में विशेष सम्बन्ध रखने वाले लोगो का मनोनयन करने की व्यवस्था
v. कनाडा के संविधान सेa. केंद्र और राज्यों के बीच कार्य विभाजन की प्रणाली
b. अवशिष्ठ शक्तियों पर केंद्र का अधिकार
c. राजयपाल की नियुक्ति प्रक्रिया
vi. ऑस्ट्रेलिया के संविधान सेa. समवर्ती सूचि की अवधारणा
b. लोकसभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक की व्यवस्था
c. संविधान में प्रस्तावना की भाषा
vii. दक्षिण अफ्रीका के संविधान सेa. संविधान में संशोधन की प्रक्रिया
b. राजयसभा सदस्यों के निर्वासन की प्रणाली
viii. रूस के संविधान सेa. मौलिक कर्तव्यों का अनुबंध
b.न्याय के मुख्य आदर्श - सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की अभिप्रेरणा
c. पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा
ix. जापान के संविधान सेa. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण की प्रेरणा
x. जर्मनी के संविधान सेa. आपात काल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित किये जाने की शक्ति का प्रावधान जर्मनी से लिया गया हैं ।
Note : ये सभी कानून या नियम भारतीय संविधान में किसी व्यक्ति विशेष की सहमति से नहीं जोड़े गए बल्कि इन पर संविधान सभा के द्वारा चर्चा की गयी तथा बहुमत के बाद इन नियमो को भारतीय संविधान में शामिल किया गया✥ भारत के मूल संविधान में 22भाग थे लेकिन आवश्यकता के आधार पर इनमें बदलाव भी हुए इन्हीं बदलावों के कारण वर्तमान के भारतीय संविधान में कुल 25भाग हैं लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है की भारतीय संविधान की ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए इनकी वरीयता में कोई बदलाव न हो इस वजह से जो भी भाग जोड़े गए उन्हें पुराने भागों के साथ जोड़ा गया ।
✥ वर्तमान के भारतीय संविधान के भाग 4A, 9A, 9B, 14A को भारतीय संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है जो की संविधान के पुराने भाग 4, 9 और 14 के अंदर ही रखे गए है ताकि मूल संविधान के भागों का क्रम यथावत बना रहे जो की भाग 1 से भाग 22 तक है । इसके अलावा मूल संविधान के भाग 7 को भारतीय संविधान के सातवें संसोधन के द्वारा 1 नवम्बर 1956 को संविधान से पृथक कर दिया गया जिसमें अनुच्छेद 238 के तहत राज्यों को तीन श्रेणियों में बांटे जाने का प्रावधान था ।
| अनुसूची | विवरण |
|---|---|
| अनुसूची संख्या 1 | इस अनुसूची में भारत देश तथा उसके राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया हैं । |
| अनुसूची संख्या 2 | इस अनुसूची में विभिन्न राजपत्रित अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में वर्णन किया गया हैं जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष आदि पद शामिल हैं । |
| अनुसूची संख्या 3 | इस अनुसूची में विभिन्न राजपत्रित अधिकारियों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदि विशिष्ट पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का विवरण दिया गया हैं । |
| अनुसूची संख्या 4 | इस अनुसूची में भारत के विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाने वाले राज्यसभा सदस्यों की सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया हैं । राज्य सभा में उतरप्रदेस से सर्वाधिक 31 सदस्य चुने जाते हैं । |
| अनुसूची संख्या 5 |
इस अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया गया हैं । इसके अतिरिक्त किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किये गये ताकि इन मानदंडों को आधार मानकर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया जा सके जो की निम्नाकित हैं - 1. किसी क्षेत्र में जनजाति की बहुलयता का होना 2. निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में उस विशेष क्षेत्र का आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की दर्ष्टि में पिछड़ापन 3. उस क्षेत्र में विशेष प्रशासनिक इकाई की उपलब्धता इस अनुसूची के तहत 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का वर्णन किया गया हैं जिनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के नाम शामिल हैं |
| अनुसूची संख्या 6 | इस अनुसूची का अनुबंध बारदोलोई समिति की सिफारिश पर किया गया था जिसके अनुसार प्रशासन की एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो की जनजातीय क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दे सके । इसी के फलस्वरूप यह अनुसुची भारत के पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में पाई जाने वाली जनजातियों के अधिकारों को सरंक्षण प्रदान करती हैं । |
| अनुसूची संख्या 7 | इस अनुसूची में संघ तथा राज्य सरकारों की कार्य शक्ति को निर्धारित/विभक्त करने के लिए 3 सूचियों का वर्णन किया है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल हैं । |
| अनुसूची संख्या 8 |
इस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओँ का वर्णन किया गया हैं जिसमें कुल 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया हैं जिनकी संख्या मूल संविधान में 14 थी । मूल संविधान की 8वीं अनुसुची में शामिल भाषाएं - 1. हिन्दी 2. कश्मीरी 3. पंजाबी 4. बंगाली 5. ओड़िया 6. असमिया 7. गुजराती 8. मराठी 9. तेलगु 10. कन्नड़ 11. तमिल 12. उर्दू 13. मलयालम 14. संस्कृत संविधान की 8वीं अनुसूची में 1967 में हुए 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिन्धी भाषा को , 1992 में हुए 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी मणिपुरी, नेपाली भाषा को तथा 2003 में हुए 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को जोड़ा गया । इस प्रकार वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22भाषाएँ हैं |
|
👆 मूल संविधान की अनुसूचियां 👇 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई अनुसूचियाँ |
|
| अनुसूची संख्या 9 |
समाजवादी नीतियों को लागु करते समय मौलिक अधिकार व्यवधान उत्पन न कर पाएं इस वजह से 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य था भूमि सुधार कानूनों को सफलताफूर्वक निष्पादित करना । इस अनुसूची में केंद्र तथा राज्य सरकारें कानून डाल सकती है और इस अनुसूची में डाले गए कानून को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती हैं । आरंभिक समय में इस अनुसूची में कुल 13 कानून शामिल किये गये थे जबकि वर्तमान समय में कुल 284 कानून इस अनुसूची के दायरे में आते हैं । गौरतलब है कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया तथा सभी लोगो के पास भूमि अधिकार सीमित मात्रा में रह गए जो की अनुच्छेद 31 के तहत असंवैधानिक कार्य था जिसके चलते ही सरकार ने इस अनुसूची को संविधान में शामिल करके यह प्रावधान कर दिया कि इस अनुसूची में शामिल किये गये कानूनों पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायालय के पास नहीं रहेगी । Note : 1980 में वामन राव बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया मामले के फैसले में सर्वोच्च न्यालय ने यह कहा की 27 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून इस अनुसूची में शामिल किये गये या शामिल किये जायेंगे उन सभी कानूनों पर न्यायालय को न्यायिक पुनर्रीक्षण का अधिकार हैं । वर्तमान समय में इस अनुसूची के कानूनों को भी न्यायालय में चुनोती दी जा सकती हैं । |
| अनुसूची संख्या 10 | इस अनुसूची में दल-बदल निषेध कानून का वर्णन किया गया है जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में शामिल किया गया था । इस कानून के अंतर्गत कोई विधायक या सांसद अपनी मर्जी से एक दल से दूसरे दल में नहीं जा सकता है और न ही सदन में अपनी पार्टी के विरुद्ध मत डाल सकता हैं यदि ऐसा किया जाता है तो उस विधायक या सांसद की सदस्य्ता रद्द कर दी जाती हैं । यदि किसी पार्टी के दो तिहाई सदस्य अथवा पूरी पार्टी ही किसी अन्य पार्टी में विलीन हो जाती है तो उस स्थिति में कोई सांसद या विधायक अपनी मर्जी से इसके विरुद्ध अपनी मर्जी से किसी अन्य पार्टी में शामिल हो सकता है उस स्थिति में उसकी सदस्यता निरस्त नहीं होगी । |
| अनुसूची संख्या 11 | 1992 में हुए 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया जिसमें पंचायतीराज व्यवस्था का वर्णन किया गया हैं । इस अनुसूची में कुल 29 विषयों का वर्णन किया गया हैं । इन 29 विषयों में से कितने विषय पंचायती राज संस्थाओं को देने है इसका निर्धारण संबंधित राज्य का विधानमंडल तय करता हैं । |
| अनुसूची संख्या 12 | 1992 में हुए 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 12वी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया जिसका सम्बन्ध नगरीय स्वशासन से हैं । इसके अंतर्गत 3 प्रकार की संस्थाएँ नगर पालिकाएं, नगर परिषद तथा नगर निगम शामिल होती हैं । इस अनुसूची में कुल 18 विषयों का वर्णन किया गया हैं । इन 18 विषयों में से कितने विषय नगरीय स्वशासन संस्थाओं को देने है इसका निर्धारण संबंधित राज्य का विधानमंडल तय करता हैं । |
जानकारी जल्द ही उपलब्ध होगी ...
जानकारी जल्द ही उपलब्ध होगी ...